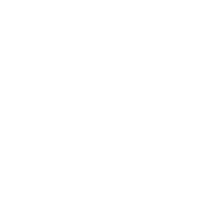Do you want to know more about
Digital Bharat Nidhi (DBN)?
Explore the FAQs below.

डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के स्थान पर स्थापित एक कोष है।
डिजिटल भारत निधि के उद्देश्य हैं:
• वंचित ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं तक पहुंच और वितरण को बढ़ावा देने के माध्यम से सार्वभौमिक सेवा का समर्थन करना।
• दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के अनुसंधान और विकास का समर्थन करना।
• उपरोक्त खंड (क) के तहत सेवा के प्रावधान के लिए पायलट परियोजनाओं, परामर्श सहायता और सलाहकार सहायता का समर्थन करना।
• दूरसंचार सेवाओं, प्रौद्योगिकियों और उत्पादों की शुरूआत का समर्थन करना।
डीबीएन का प्रशासन भारत की केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि) नियम, 2024 के खंड 3 में डीबीएन के प्रशासक की शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए हैं।
दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि) नियम, 2024 के खंड 5 में डीबीएन के तहत योजनाओं और परियोजनाओं को शुरू करने के लिए मानदंड प्रदान किए गए हैं।
दूरसंचार अधिनियम, 2023 में प्रावधान है कि डिजिटल भारत निधि के लिए कोई भी धनराशि जो दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 3 के तहत प्राधिकरण के अनुसार भुगतान की जाती है, उसे डिजिटल भारत निधि में जमा किया जाएगा। वित्तीय वर्ष के अंत में डीबीएन के खाते में जमा राशि समाप्त नहीं होती है।
देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के प्रावधान के लिए सार्वभौमिक सेवा समर्थन नीति 01.04.2002 से लागू हुई। दिसंबर 2003 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 ने सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) को वैधानिक दर्जा दिया। इसके बाद, 29.12.2006 को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में विभिन्न टेलीग्राफ सेवाओं (मोबाइल सेवाओं, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और OFC जैसी अवसंरचना के निर्माण सहित) तक पहुँच प्रदान करने के लिए USOF का दायरा बढ़ गया।
डीबीएन को, अन्य बातों के साथ-साथ, वंचित ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा की पहुंच और वितरण को बढ़ावा देने के माध्यम से सार्वभौमिक सेवा का समर्थन करने का अधिदेश दिया गया है, जबकि पूर्ववर्ती यूएसओएफ को ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को टेलीग्राफ सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने का अधिदेश दिया गया था।
दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अनुसार, सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओएफ) के लिए नियत दिन से पहले दिए गए लाइसेंस के तहत देय सभी राशियां, डिजिटल भारत निधि के लिए देय राशियां मानी जाएंगी।
डीबीएन से संबंधित गतिविधियों का कार्यान्वयन "कार्यान्वयनकर्ताओं" द्वारा किया जाता है, अर्थात वे संस्थाएं जिनके पास दूरसंचार सेवाएं या बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार/दूरसंचार विभाग से वैध लाइसेंस या पंजीकरण या प्राधिकरण है या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य संस्थाएं हैं।
प्रमुख डीबीएन परियोजनाएं हैं:
- भारतनेट और संशोधित भारतनेट कार्यक्रम
- मोबाइल टावर परियोजनाएँ
- 4G संतृप्ति परियोजना
- आकांक्षी जिलों में 7287 अछूते गांव
- आकांक्षी जिलों में 502 अछूते गांव
- 354 अछूते गांव
- आकांक्षी जिलों में 502 अछूते गांव,
- वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों (चरण I और II) में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान,
- NER (NESA) में मोबाइल सेवाएं
- अरुणाचल प्रदेश और असम के 2 जिलों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान
- मेघालय में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान
- BOP/BIP
- ANI में मोबाइल सेवाएं
- इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना लक्षद्वीप
- द्वीपों में पनडुब्बी ओएफसी कनेक्टिविटी
- दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीटीडीएफ)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25.10.2011 को देश की सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) में गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) परियोजना को मंजूरी दी। इसके बाद, एनओएफएन परियोजना का नाम बदलकर भारतनेट कर दिया गया। भारतनेट परियोजना के तहत बनाया गया बुनियादी ढांचा एक राष्ट्रीय संपत्ति है।
परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, भारतनेट को लागू करने के लिए एक संशोधित रणनीति को 19.07.2017 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए मीडिया (ओएफसी/रेडियो/सैटेलाइट) का एक इष्टतम मिश्रण प्रदान करता है; ब्लॉक से जीपी तक नए फाइबर बिछाए जाते हैं, और सभी जीपी में अंतिम मील वास्तुकला की स्थापना की जाती है।
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) है, जिसे भारत सरकार द्वारा संचार और आईटी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) की स्थापना, प्रबंधन और संचालन के लिए स्थापित किया गया है। बीबीएनएल को 25-02-2012 को कंपनी अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) / कंपनी के रूप में शामिल किया गया है।
राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) की स्थापना, प्रबंधन और संचालन का कार्य जारी रखना, जिसकी परिकल्पना भारत सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायतों को उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए की गई है।
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) का भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के साथ विलय कर दिया गया है। इस विलय का उद्देश्य ग्रामीण भारत में भारतनेट नेटवर्क को तेजी से शुरू करना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 04.08.2023 को रिंग नेटवर्क में भारतनेट चरण-I और चरण-II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन, शेष 47,000 ग्राम पंचायतों (लगभग) में नेटवर्क के निर्माण, 10 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव तथा उपयोग के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी। लगभग 3.8 लाख (लगभग) गैर-ग्राम पंचायत गांवों को उनकी संबंधित ग्राम पंचायतों से मांग के आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रस्ताव है। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के लिए बीएसएनएल को परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
भारतनेट चरण-I को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) - भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (रेलटेल) और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के मौजूदा फाइबर का उपयोग करके जीपीओएन (गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क) तकनीक के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है और ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी अंतर को पाटने के लिए भूमिगत वृद्धिशील फाइबर बिछाया गया है।
मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई, 2017 को भारतनेट के लिए संशोधित रणनीति को मंजूरी दी, जो परियोजना के चरण-I के कार्यान्वयन अनुभव को एकीकृत करती है और इसे डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के साथ जोड़ती है। संशोधित रणनीति ग्राम पंचायतों (जीपी) को जोड़ने के लिए मीडिया (ओएफसी/रेडियो/सैटेलाइट) का इष्टतम मिश्रण प्रदान करती है, प्रत्येक जीपी को 1 जीबीपीएस बैंडविड्थ (वायर्ड मीडिया पर) प्रदान किया जाएगा, जीपी और ब्लॉक के बीच नए फाइबर बिछाए जाएंगे, कई कार्यान्वयन मॉडल - राज्य-आधारित मॉडल, निजी क्षेत्र और सीपीएसयू मॉडल, साथ ही वाई-फाई या किसी अन्य उपयुक्त ब्रॉडबैंड तकनीक के माध्यम से जीपी में अंतिम मील कनेक्टिविटी।
भारतनेट चरण-II का कार्यान्वयन निम्नलिखित मॉडल के तहत किया गया:
- राज्य-नेतृत्व मॉडल: आठ राज्य अर्थात् छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना इस मॉडल के तहत कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
- बीबीएनएल के नेतृत्व वाला निजी मॉडल: दो राज्यों अर्थात् पंजाब और बिहार को बीबीएनएल द्वारा सीधे निजी क्षेत्र के मॉडल के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
- सीपीएसयू: इस मॉडल के तहत, बीएसएनएल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और सिक्किम में कार्यों को क्रियान्वित कर रहा है जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
- उपग्रह: चरण- II का उपग्रह घटक बीएसएनएल और बीबीएनएल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- लगभग 1.64 लाख ग्राम पंचायतों (राज्य संचालित मॉडल के अंतर्गत 53,265 ग्राम पंचायतों को छोड़कर) का उन्नयन करना तथा शेष लगभग 47 के ग्राम पंचायतों (सैटेलाइट ग्राम पंचायतों सहित) का निर्माण करना।
- ब्लॉक तथा जी.पी.एस. पर आई.पी.-एम.एल.एस. नेटवर्क, जिसमें ब्लॉकों में 10 जी.बी.पी.एस. डाउनवर्ड लिंक तथा जी.पी.एस. पर 1 जी.बी.पी.एस. डाउनवर्ड लिंक के साथ राउटर का प्रावधान है।
- लगभग 2.64 लाख ग्राम पंचायतों का संचालन एवं रखरखाव, जिसमें नेटवर्क अपटाइम 99% (के.पी.आई. आधारित) है।
- बीएसएनएल सभी 7,269 ब्लॉकों में इंटरनेट लीज्ड लाइन (आई.एल.एल.) बैंडविड्थ उपलब्ध कराएगा।
- भारतनेट उद्यमी मॉडल के माध्यम से अंतिम-मील नेटवर्क का क्रियान्वयन किया जाएगा।
- प्रत्येक एफ.टी.टी.एच. ग्राहक के लिए न्यूनतम 25 एम.बी.पी.एस. डाउनलोड स्पीड।
- एक करोड़ पचास लाख ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराना। पांच (5) वर्षों की अवधि में ग्रामीण परिवारों/संस्थाओं/उद्यमों में लाख (1.5) करोड़ एफटीटीएच कनेक्शन।
रोलआउट योजना (संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के साथ संरेखित) निम्नानुसार है:
- प्रारंभिक चरण में, उच्च नेटवर्क अपटाइम (>=90%) वाले लगभग 51,000 ग्राम पंचायतों में माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को एफटीटीएच कनेक्शन से जोड़ा जाएगा।
- जिन ग्राम पंचायतों में नेटवर्क अपटाइम <90% है, वहां के माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को नेटवर्क अपटाइम >90% करने के बाद एफटीटीएच से जोड़ा जाएगा।
- जिन ग्राम पंचायतों में नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, वहां के माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को बाद में संशोधित भारतनेट के तहत भारतनेट नेटवर्क के निर्माण के अनुसार जोड़ा जाएगा।
बीएनयू एक स्थानीय चैम्पियन है, जो ग्राम स्तर का उद्यमी, इंटरनेट सेवा प्रदाता, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) आदि हो सकता है।
भारतनेट उद्यमियों (बीएनयू) मॉडल के तहत, भारतनेट उद्यमियों का उपयोग गांव से लेकर घर तक अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करने और बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। नए घरेलू फाइबर कनेक्शन सक्रिय करने के लिए बीएनयू को एकमुश्त वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।
निजी कम्पनियां निम्नलिखित तरीकों से भाग ले सकती हैं:
- भारतनेट से बैंडविड्थ और फाइबर लीज पर लेना।
- वाई-फाई और फाइबर-टू-द-होम (FTTH) जैसे अंतिम-मील कनेक्टिविटी समाधान स्थापित करना।
भारतनेट डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है:
- ई-गवर्नेंस सेवाएँ
- डिजिटल भुगतान और बैंकिंग पहुँच
- ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा (टेलीमेडिसिन)
- दूरस्थ कार्य और ई-कॉमर्स के अवसर
- डिजिटल कक्षाओं को सक्षम बनाता है
- स्कूलों और छात्रों को इंटरनेट पहुँच प्रदान करके ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफ़ॉर्म और दूरस्थ शिक्षा
FTTH का मतलब है फाइबर टू द होम, और यह एक प्रकार का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जो फाइबर-ऑप्टिक केबल का उपयोग करके सीधे घर या इमारत में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाता है। FTTH तेज़ डाउनलोड/अपलोड गति, अधिक विश्वसनीयता और कम विलंबता प्रदान करता है, जो इसे स्ट्रीमिंग, गेमिंग, वीडियो कॉल और स्मार्ट होम डिवाइस चलाने जैसी गतिविधियों के लिए आदर्श बनाता है।
नेटवर्क को आईपी-एमपीएलएस का उपयोग करके रिंग आकार में बनाया गया है, इसलिए यदि एक पथ विफल हो जाता है, तो डेटा दूसरा मार्ग ले सकता है, जिससे एक स्थिर और विश्वसनीय कनेक्शन सुनिश्चित होता है।
मोबाइल टावर, जिसे सेल टावर या बेस स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी संरचना है जिसमें मोबाइल डिवाइस (जैसे सेल फोन और टैबलेट) और मोबाइल नेटवर्क के बीच वायरलेस संचार के लिए आवश्यक रेडियो उपकरण रखे जाते हैं। यह सेल सिग्नल उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण रिले पॉइंट के रूप में कार्य करता है।
यह कैसे काम करता है इसका सरलीकृत विवरण इस प्रकार है:
- सिग्नल ट्रांसमिशन: आपका मोबाइल डिवाइस निकटतम मोबाइल टावर को रेडियो सिग्नल भेजता है। इस सिग्नल में आपके कॉल, टेक्स्ट मैसेज या डेटा उपयोग के बारे में जानकारी होती है।
- टावर रिसेप्शन: टावर का एंटीना इस सिग्नल को प्राप्त करता है और इसे फाइबर ऑप्टिक केबल या माइक्रोवेव लिंक के माध्यम से मोबाइल नेटवर्क के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचाता है।
- नेटवर्क प्रोसेसिंग: नेटवर्क आपके अनुरोध को प्रोसेस करता है (उदाहरण के लिए, आपके कॉल को कनेक्ट करता है, वेबपेज को पुनः प्राप्त करता है)।
- सिग्नल रिटर्न: प्रतिक्रिया नेटवर्क के माध्यम से टावर को वापस भेजी जाती है।
- डिवाइस रिसेप्शन: टावर का एंटीना आपके मोबाइल डिवाइस को सिग्नल को फिर से भेजता है।
अनिवार्य रूप से, मोबाइल टावर एक उच्च-शक्ति वाले रिपीटर के रूप में कार्य करता है, जो नेटवर्क के सिग्नल की सीमा को बढ़ाता है और उपकरणों और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच संचार को सुविधाजनक बनाता है। एक ही टावर पर कई एंटेना अलग-अलग आवृत्तियों और नेटवर्क तकनीकों (जैसे 4G, 5G) को संभाल सकते हैं।
1990 के दशक में, 2G ने डिजिटल वॉयस ट्रांसमिशन के साथ एक बड़ा अपग्रेड लाया, जिससे GPRS और EDGE जैसी तकनीकों के माध्यम से टेक्स्ट मैसेजिंग (SMS) और बुनियादी इंटरनेट सेवाएँ सक्षम हुईं। 2000 के दशक की शुरुआत में 3G का उदय हुआ, जिसने मोबाइल ब्रॉडबैंड की शुरुआत की, जिससे तेज़ इंटरनेट एक्सेस, वीडियो कॉलिंग और मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग की अनुमति मिली, जिसकी स्पीड 2 Mbps तक पहुँच गई। फिर 2010 के दशक में 4G आया, जिसने काफी तेज़ गति (1 Gbps तक) और कम विलंबता की पेशकश की, जिससे HD वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और वॉयस ओवर LTE (VoLTE) संभव हो पाया। अंत में, 5G, जो 2020 के दशक में शुरू हुआ, एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है, जो अल्ट्रा-फास्ट स्पीड (1-10 Gbps), अविश्वसनीय रूप से कम विलंबता और अरबों डिवाइस को जोड़ने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे स्मार्ट सिटी, स्वायत्त वाहन और इमर्सिव AR/VR अनुभव जैसे नवाचारों को बल मिलता है।
डीबीएन देश में दूरसंचार सेवाओं में सुधार के लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, जैसे भारतनेट, 4जी संतृप्ति परियोजना, आकांक्षी जिलों के कवर न किए गए क्षेत्रों में मोबाइल सेवा का प्रावधान, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं, हिमालयी और सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं, द्वीपों में मोबाइल सेवाएं, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं, मेघालय में मोबाइल सेवाएं, अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों में मोबाइल सेवाएं आदि।
डीबीएन योजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति डीबीएन की वेबसाइट (www.usof.gov.in) पर उपलब्ध है।
इस परियोजना के तहत दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में सभी कवर किए गए गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। परियोजना में पुनर्वास, नई बस्तियों, मौजूदा ऑपरेटरों द्वारा सेवाओं को वापस लेने आदि के कारण अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान है।
आकांक्षी जिलों के लिए डीबीएन द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:
- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 7,287 आकांक्षी जिला गांव: इस परियोजना के तहत पांच राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- आकांक्षी जिला के 502 गांव (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार): चार राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान) के 112 आकांक्षी जिलों के 502 गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने की योजना को अंतिम रूप दिया गया है।
वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी चरण-I वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। इस परियोजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में संचार और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना में बेहतर कनेक्टिविटी और इंटरनेट सेवाओं के लिए एलडब्ल्यूई चरण-I के तहत मौजूदा 2जी मोबाइल टावरों को 4जी तकनीक में अपग्रेड करना शामिल है।
वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी चरण-II, चरण-I का विस्तार है, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के अधिक दूरदराज और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों तक मोबाइल कवरेज का विस्तार करता है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी-एनईआर) का उद्देश्य असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे और दूरदराज के गांवों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराना है।
इस योजना का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों (कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ) के दूरसंचार सुविधा से वंचित गांवों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे इन क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना में वृद्धि होगी।
मेघालय के कवर न किए गए गांवों और राष्ट्रीय राजमार्गों में 4जी आधारित मोबाइल सेवाओं का प्रावधान ग्रामीण और राजमार्ग गलियारों में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार लाने पर केंद्रित है।
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में चिन्हित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वंचित गांवों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 4जी मोबाइल सेवाएं शुरू करने से इस सुदूर केंद्र शासित प्रदेश में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24.03.2023 को बीएसएनएल को नामांकन के आधार पर भारतीय सीमा सुरक्षा बलों की सीमा चौकियों (बीओपी) और आईबी की सीमा खुफिया चौकियों (बीआईपी) के 1,117 स्थानों पर 4जी आधारित मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए परियोजना को मंजूरी दी है।
कार्यों में शामिल हैं:
- 17 मौजूदा 2G टावर साइटों को 4G मोबाइल सेवाओं में अपग्रेड करना।
- 4G मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए अतिरिक्त 20 नए मोबाइल टावर साइटों (सुहेली द्वीप सहित) की स्थापना।
- लक्षद्वीप द्वीपसमूह में FTTH के प्रावधान के लिए 225 किलोमीटर OFC नेटवर्क का निर्माण। इसमें 10 साल के लिए समान QoS/SLA पर सेवाओं के प्रावधान के साथ 5 साल के लिए संचालन और रखरखाव लागत शामिल है।
31.03.2025 तक डीबीएन के अंतर्गत 18,305 टावर लगाए गए, जिनसे 24,678 गांव कवर हुए।
डिजिटल भारत निधि (DBN) पहल के हिस्से के रूप में इंट्रा सर्किल रोमिंग (ICR) नियम, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSP) को सरकार द्वारा वित्तपोषित मोबाइल टावरों पर बुनियादी ढांचे को साझा करने की अनुमति देते हैं। इसका मतलब है कि जियो, एयरटेल और बीएसएनएल जैसे विभिन्न TSP के उपयोगकर्ता DBN द्वारा वित्तपोषित टावरों पर अन्य TSP के बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर 4G नेटवर्क तक पहुँच सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, भले ही वे अपने टावर के कवरेज क्षेत्र से बाहर हों।
द्वीपों के लिए सीटीडीपी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप में दूरसंचार संपर्क बढ़ाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है:
- हाई-स्पीड इंटरनेट के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC)
- इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए बैंडविड्थ वृद्धि
- बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 4G मोबाइल सेवाओं का विस्तार
यह परियोजना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए शुरू की गई:
- दूरस्थ द्वीप क्षेत्रों में संचार अवसंरचना में सुधार
- निवासियों, व्यवसायों और पर्यटकों को बेहतर इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करें
- ऑनलाइन शिक्षा, ई-गवर्नेंस और स्वास्थ्य सेवा जैसी डिजिटल सेवाओं का समर्थन करें
डीबीएन एएनआई और लक्षद्वीप द्वीपसमूहों सहित देश के दूरदराज के द्वीपों में डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए विभिन्न परियोजनाओं को लागू कर रहा है जैसे सीएएनआई (चेन्नई अंडमान निकोबार द्वीपसमूह) पनडुब्बी ओएफसी परियोजना, केएलआई (कोच्चि से लक्षद्वीप) पनडुब्बी ओएफसी परियोजनाएं, कवर किए गए गांवों के लिए 4 जी एएनआई परियोजना और एनएच -4, 4 जी संतृप्ति परियोजना, 4 जी संतृप्ति परियोजना, भारतनेट परियोजना, लक्षद्वीप में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, उपग्रह बैंडविड्थ वृद्धि आदि।
चेन्नई पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों से जुड़ा हुआ है, जिनमें स्वराज द्वीप (हैवलॉक), लॉन्ग आइलैंड, रंगत, लिटिल अंडमान (हुतबे), कामोर्टा, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार (कैम्पबेल बे) शामिल हैं।
कोच्चि-लक्षद्वीप पनडुब्बी ओएफसी परियोजना कावारत्ती और लक्षद्वीप के दस अन्य द्वीपों, अर्थात् कल्पेनी, अगत्ती, अमिनी, एंड्रोथ, मिनिकॉय, बांगरम, बितरा, चेटलाट, किल्टान और कदमत को जोड़ती है।
संचार मंत्रालय द्वारा 01 अक्टूबर, 2022 को दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीटीडीएफ) योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य भारत में दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए शिक्षाविदों, स्टार्ट-अप्स, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण-विशिष्ट संचार प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) को वित्तपोषित करना है।
टीटीडीएफ निम्नलिखित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:
- अल्पसुविधा प्राप्त क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार करके डिजिटल विभाजन को पाटना।
- आयात पर निर्भरता कम करने के लिए दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास को प्रोत्साहित करना।
- उन्नत दूरसंचार समाधान विकसित करने में स्टार्टअप, एमएसएमई और अनुसंधान संस्थानों का समर्थन करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
टीटीडीएफ माननीय प्रधानमंत्री के "जय अनुसंधान" के दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है और इसका उद्देश्य स्वदेशी दूरसंचार समाधानों को बढ़ावा देना है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकी विकसित करने तथा दूरसंचार उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए भारतीय संस्थाओं को अनुदान।
- दूरसंचार प्रौद्योगिकी और समाधानों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।
- आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यावसायीकरण।
- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में किफायती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं को सक्षम बनाना।
- बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) का निर्माण।
- परियोजना कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक सुपरिभाषित प्रक्रिया।
- पारदर्शी मूल्यांकन और अनुमोदन मानदंड।
- आयात को कम करते हुए निर्यात के अवसर खोलना।
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानक निकायों में योगदान।
आप निम्न लिंक पर जाकर टीटीडीएफ दिशानिर्देश देख सकते हैं: https://ttdf.usof.gov.in/assets/pdf/ttdf_guidelines.pdf.
सरकार ने डीबीएन वित्त पोषित योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं और ब्रॉडबैंड के विस्तार के लिए कई कदम उठाए हैं और चरणबद्ध तरीके से देश के सभी हिस्सों में कवरेज प्रदान करने की योजना है।
भारी वित्तीय लागत के कारण सभी कवर न किए गए गांवों को एक परियोजना में शामिल नहीं किया जा सकता है, साथ ही विभिन्न ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए विभिन्न तकनीकी अध्ययन किए जाने की भी आवश्यकता है।
इंटरनेट कनेक्शन एक डेटा कनेक्शन है जो इंटरनेट एक्सेस सहित इंटरैक्टिव सेवाओं का समर्थन करने में सक्षम है। भारत में, 2 एमबीपीएस की न्यूनतम डाउनलोड स्पीड की क्षमता वाले इंटरनेट कनेक्शन को ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहा जाता है।
इंटरनेट सेवाएं वायरलेस एक्सेस जैसे 2जी, 3जी, 4जी, वाई-फाई और वायरलाइन जैसे एफटीटीएच/कॉपर केबल कनेक्शन और सैटेलाइट के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।
सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा डीबीएन के लिए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 5% योगदान दिया जा रहा है।
अगस्त 2023 में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के तहत अगले पांच वर्षों में 1.50 करोड़ एफटीटीएच कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। भारतनेट उद्यमी (बीएनयू) ब्लॉक और जीपी स्तर पर स्थानीय उद्यमियों को तैयार करने के लिए विभाग की एक पहल है, जो देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट क्रांति फैलाएंगे। यह स्थानीय व्यक्ति के लिए एक बेहतरीन व्यवसायिक अवसर है, जो रोजगार भी पैदा कर सकता है और अपने करियर से जुड़े सपने भी पूरे कर सकता है। बीएनयू मॉडल के तहत, दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी)/इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) आपसी सहमति से राजस्व साझाकरण व्यवस्था के अनुसार भारतनेट के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में एफटीटीएच कनेक्शन के प्रसार के लिए आईसीटी ज्ञान रखने वाले स्थानीय उद्यमियों के साथ साझेदारी कर सकते हैं।
अधिदेश के अनुसार, डीबीएन ग्रामीण, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की पहुंच और वितरण को बढ़ावा देने के माध्यम से सार्वभौमिक सेवा का समर्थन करता है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, नई योजनाओं की योजना बनाई गई है और मुख्य रूप से हाशिए के समुदायों और ग्रामीण क्षेत्रों सहित समाज के सभी वर्गों के लिए समावेशी और सुलभ हैं।
बैकहॉल या एक्सचेंज बैकहॉल, वह सबनेटवर्क है जो डेटा सेंटर को स्थानीय एक्सचेंज से जोड़ता है। ये एक्सचेंज आमतौर पर स्ट्रीट कैबिनेट से जुड़े होते हैं, जो कॉपर या फाइबर ऑप्टिक केबल द्वारा आपके राउटर से जुड़ते हैं, जो आपके कार्यालय या घर तक इंटरनेट पहुंचाते हैं। बैकहॉल का उपयोग मोबाइल डेटा एक्सेस के लिए भी किया जाता है।